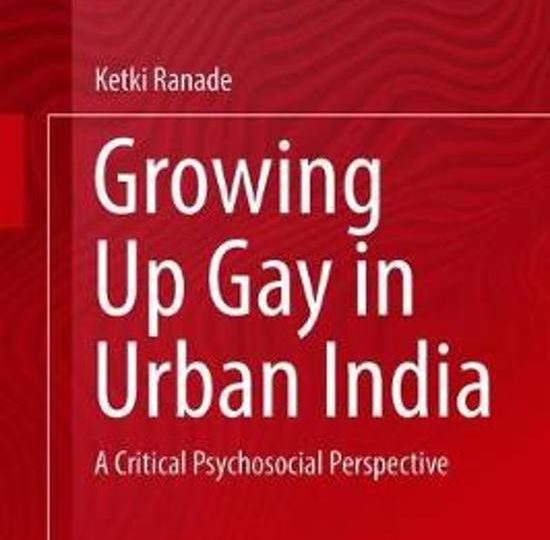
डॉक्टर केतकी रानाडे की पुस्तक, ग्रोईंग अप गे इन अर्बन इंडिया – अ क्रिटिकल साइकोसोशल पर्सपेक्टिव (प्रकाशक – स्प्रिंगर नेचर, सिंगापुर 2018) की समीक्षा
“हमेशा कुछ उपयोगी सीखने की इच्छा करते रहना चाहिए” – सोफॉक्लीज़”
डॉक्टर केतकी रानाडे के साथ मेरा संपर्क आज से लगभग 18 वर्ष पहले उनकी मनोरोग और सामाजिक कार्य विषय पर डिग्री की पढ़ाई के दौरान हुआ था। इन पिछले 18 वर्षों के दौरान मुझे डॉक्टर रानाडे द्वारा लेस्बियन, गे, बाइ-सेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर और क्विअर (LGBTQ) लोगों के साथ समर्पित भाव और पूरे जोश के साथ किए जा रहे कार्यों की जानकारी रही है। डॉक्टर रानाडे की यह नई किताब, ‘ग्रोईंग अप गे इन अर्बन इंडिया – अ क्रिटिकल साइकोसोशल पर्सपेक्टिव’, 80 और 90 के दशक में उनके द्वारा मुंबई और पुणे में रह रहे समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं के जीवन पर किए गए अनुसंधान से मिले अनुभवों पर आधारित है। डॉक्टर रानाडे की इस किताब से हमें भारतीय शहरों में रहने वाले समलैंगिक, बाइ-सेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर और क्विअर लोगों के जीवन के भावनात्मक अनुभवों और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में दुर्लभ अंतर्दृष्टि मिलती है।
इस किताब को लिखने की प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर रानाडे ने अनेक लोगों के साथ इंटरव्यू किए और इन लोगों के अनुभवों को मनो-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की है। किताब की शुरुआत में बच्चों और किशोरों की विकास प्रक्रिया, विशेषकर उनकी यौन पहचान के विकास को समझने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली व्यवस्था की समालोचना शामिल है। इस व्यवस्था की समालोचना में डॉक्टर रानाडे ने समलैंगिक पहचान के विकास के बारे में किसी भी तरह के लिखित साहित्य के अभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
किताब का दूसरा अध्याय डॉक्टर रानाडे द्वारा अनुसंधान के लिए अपनाई गयी विधि से हमें परिचित करवाता है। उनके द्वारा अपनाए गए तरीके में अनुसंधान में शामिल लोगों द्वारा दी गयी जानकारी को आधार बना कर उन लोगों की इस उभरती हुई समलैंगिक पहचान के बारे में उनके अनुभवों को समझने का प्रयास किया गया है। अनुसंधान के लिए उनके द्वारा अपनाई गयी यह प्रक्रिया, आमतौर पर दो तरह के जेंडर, अर्थात महिला और पुरुष मानसिकता या विषमलैंगिकता के विकास को समझने की प्रक्रिया से भिन्न है। उनके अनुसंधान में पूर्वी और पश्चिमी देशों के लोगों की संस्कृति के अंतर पर भी ध्यान दिया गया है क्योंकि अभी तक इस विषय पर हुए सभी अनुसंधान और उपलब्ध साहित्य यूरोप और अमरीकी लोगों के दृष्टिकोणों पर आधारित रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर रानाडे का स्पष्टीकरण इस प्रकार है, ““इस तरह की अनुसंधान प्रक्रिया को अपनाने का यह अर्थ कदापि नहीं है या मैंने ऐसा कोई सुझाव नहीं देने की कोशिश की है कि व्यक्तियों के निजी अनुभवों और किसी समूह के अनुभवों में अंतर होता है या फिर पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के बीच किसी तरह का कोई अंतर है। आज की इस वैश्विक व्यवस्था में जहाँ एक ओर इस तरह के अंतर कर पाना संभव नहीं है, वहीं यह भी सही है कि हर संस्कृति में लोगों के अपने अनुभव, उस संस्कृति के अनुभवों से अलग हो सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि सिन्हा व त्रिपाठी (2003) द्वारा सुझाया गया है, ‘व्यक्तिगत’ और ‘सामूहिक’ विचार, रुझानों की तरह होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति और संस्कृति में एक ही समय पर पाए जाते हैं और अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में उजागर होते हैं। किताब के इस अध्याय में और किताब में बाद में भी मैंने अपने अनुसंधान के विश्लेषण के लिए भारतीय संदर्भ में हुए अनेक ऐसे अनुसन्धानों का हवाला दिया है जो सामाजिक और पारिवारिक विचार व्यवस्था में भी निजी विचार बनने और समायोजित होने का समर्थन करते हैं। (अध्याय 1, फूटनोट 7, पृष्ठ 23)
किताब के तीसरे से छ्ठे अध्याय में इस अनुसंधान में शामिल लोगों के अनेक मार्मिक जीवन अनुभव शामिल किए गए हैं जिनसे हमें इनके संघर्षों के बारे में पता चलता है। लोगों के अनुभवों में उनकी नई उजागर होती समलैंगिक पहचान से जुड़े संघर्ष के बारे में और स्वीकृति खोजने और पाने के उनके प्रयासों के बारे में बताया गया है, कैसे उन्होंने सामाजिक बदलाव लाने और सक्रियता की राजनीति में शामिल होने के लिए अपनी यौनिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और सामूहिक पहचान को मजबूत किया।
अपनी किताब के अंतिम अध्याय में डॉक्टर रानाडे ने किताब में सुझाए गए उन चार मुख्य प्रस्तावों का सारांश प्रस्तुत किया है जिनके प्रयोग से व्यक्ति की पहचान और रुझानों के विकास की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गयी है। इन्हीं चार सैद्धांतिक प्रस्तावों के प्रयोग से विशिष्ट क्विअर समुदायों में युवा लोगों के अनुभवों में अंतर को जानने की कोशिश की गयी है और अंत में प्रत्येक व्यक्ति के निजी मनो-वैज्ञानिक और सामाजिक परिवेश के आधार पर इन अनुभवों की विशिष्टता उभारने की कोशिश की गयी है। इसके बाद, अनुसंधान और अध्यनन में प्रयोग किए गए तरीकों की सीमितता और सीमाओं को स्वीकार करते हुए भविष्य में एलजीबीटी क्विअर समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं पर ध्यान देने के लिए होने वाले अनुसन्धानों पर विचार व्यक्त किए गए हैं।
किताब के समापन अध्याय में इसे लिखे जाने के उद्देश्यों को फिर से दोहराया गया है, अर्थात ““मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, बाल्यकाल अध्यनन और भारत में परिवार की परंपरा को समझने की विधा के भीतर ही एक नए संवाद को शुरू करना और इनमें विधमान भेदभाव और अलगाव को समझना…अधिक समावेशी पारिवारिक और शैक्षणिक परिवेश तैयार करने के लिए नए प्रयासों का विकास करना, शिक्षाविदों, डाक्टरों, अध्यापकों, सलाहकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए ऐसे नए समावेशी पाठ्यक्रम तैयार करना जिसमें समलैंगिक रुझानों के बारे में विचार और जानकारी शामिल की गयी हो और साथ ही साथ इस क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों के लिए विषय-वस्तु तैयार करना।”“ (अध्याय 7, पृष्ठ 167-168)
इस किताब को पूरा पढ़ लेने के बाद मेरे मन में उठने वाला सबसे पहला विचार, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यह किताब विकास की प्रक्रिया को समझने, उसे गति देने के प्रति समर्पित है। इस पुस्तक का ध्यान मनुष्य के विकसित होने की इच्छा के प्रति समर्पित है क्योंकि मनुष्य की इसी इच्छा से आपसी प्रेम प्रस्फुट्टित होता है और हममें मानवीय भाव उत्पन्न होते हैं। यह केवल किताब में अध्याओं के क्रम व इसकी संरचना से ही नहीं, बल्कि अध्यनन में शामिल विभिन्न सहभागियों द्वारा दी गयी जानकारी से भी विदित होता है, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने संबंध बनाने और समुदाय के रूप में संगठित होने के बाद समाज और परिवार की तथाकथित सामान्य और स्वीकार्य परिभाषा पर सवाल उठाने शुरू किए।
किताब के आरंभिक अध्यायों में आगे आने वाले विस्तृत अनुभवों को एक संदर्भ प्रदान किया गया है। अध्यनन में शामिल लोगों द्वारा दी गयी जानकारी से हमें इन लोगों के उस संघर्ष और समाज में उनके अदृश्य बने रहने की विवशता का पता चलता है जिसका अनुभव इन्हें अपने बचपन, बाल्यकाल, युवावस्था या वयस्क जीवन के दौरान तब हुआ होगा जब पहले-पहल इन्होंने अपने व्यक्तित्व में उभर रहे इस नए यौन रुझानों को महसूस किया होगा। किताब में शामिल अनेक अनुभवों में सहभागियों ने बताया है कि अपनी यौनिक पहचान के बारे में पता चलने के बाद, जब वे इस प्रश्न से जूझ रहे थे कि “मैं ही क्यों?”” तब कैसे उन्हें एकाकीपन, अलगाव और आंतरिक और/या बाह्य मनो-सामाजिक कारणों के चलते अपनी यौनिकता को नकारने के भाव का सामना करना पड़ा।
एक ‘नो मैन्स लैंड’ में अटके होने या अधर में लटके होने की दुर्दशा, आत्म-घृणा, न केवल माता-पिता और प्रियजनों द्वारा, बल्कि अपने स्वयं के मन और शरीर के प्रति भी घृणा और विश्वासघात की संबद्ध भावना का मार्मिक चित्रण अध्ययन प्रतिभागियों में से एक के द्वारा वर्णित अनुभव में मिलता है ‘मुझे लगता है कि मेरे आरंभिक जीवन के दौरान मेरी मनोदशा बिलकुल त्रिशंकु के समान हो गयी थी (यहाँ त्रिशंकु, हिंदु पौराणिक कथाओं में वर्णित वह राजा हैं जो स्वर्ग और धरती के बीच अधर में लटके रहकर जीवन बिताने के लिए अभिशप्त थे)। इस समय में मुझे अपने इस जीवन से संबंधित रहते हुए भी अलग होने, सबके साथ होते हुए भी सबसे दूर होने का एहसास लगतार होता रहता था……” (अध्याय 3, पृष्ठ 61)
किताब में शामिल अधिकांश लोगों के अनुभवों से पता चलता है कि गैर-विषमलैंगिक यौनिक पहचान के उद्भव एवं स्वीकृति का मार्ग, उत्पीड़न की आशंका से उपजी चिंता, हिंसा और कलंकित जीवन जीने के अनुभवों से भरा पड़ा है। जब वे समाज द्वारा अपेक्षित / स्वीकार्य और आदर्श मानी जाने वाली विषमलैंगिक यौन पहचान से अलग होने के यथार्थ को स्वीकार कर लेते हैं तो वे – व्यक्तिगत, सामाजिक और सामूहिक रूप से – अपने लिए एक ऐसी नई पहचान अपना लेते हैं जो उनकी इस क्विअर पहचान को सुशोभित कर उसे मान्यता भी प्रदान करती है।
इस किताब को लिखे जाने के पीछे डॉक्टर रानाडे का उद्देश्य यह था कि भारत में स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के विषय पर एक बहुत ज़रूरी संवाद की शुरुआत की जा सके। किताब लिखने में प्रयुक्त तरीका और लेखन शैली उनके इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत हद तक सहायक रही है। हालांकि किताब के शुरुआती दो अध्यायों में इस विषय पर उपलब्ध साहित्य के अनेक संदर्भ दिये गए हैं जो उन पाठकों को आरंभ में काफ़ी कठिन लग सकते हैं जो इस विषय से अनभिज्ञ हैं या फिर वैज्ञानिक अभिलेखों को पढ़ने का अनुभव न रखते हों लेकिन बाद के अध्यायों में सहभागियों के शामिल किए गए अनुभव, इसे पढ़ने और इसके सार को ग्रहण करने को सरल कर देते हैं। कुल मिलाकर मैं इस पुस्तक को उन पाठकों के द्वारा पढ़े जाने की सिफ़ारिश करूंगी जो दूसरों के अनुभवों को समझने की सच्ची और वास्तविक इच्छा रखते हों, चाहे ये पाठक अभिभावक, भाई-बहन, बच्चे, मित्र या सहकर्मी हों अथवा नितांत अजनबी!
सोमेन्द्र कुमा द्वारा अनुवादित
To read this article in English, please click here.